
ईस्ट इंडिया कंपनी का आंतरिक प्रशासन और विनियमन सभी सरकारी नौकरी परीक्षाओं और यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यहां यूपीएससी के लिए आंतरिक प्रशासन और विनियमन पर नोट्स दिए गए हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में
- शासन की शुरूआत : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, शुरुआत में इसकी कल्पना एक व्यापारिक इकाई के रूप में की गई थी लेकिन 1765 तक यह एक शासी प्राधिकरण में बदल गई।
- घरेलू मामलों में हस्तक्षेप: 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) हासिल कर लिया। समय के साथ, इसने धीरे-धीरे भारत के आंतरिक मामलों पर अतिक्रमण कर लिया।
- प्रभुत्व का प्रयोग: 1765 से 1772 तक की समयावधि में शासन संरचना में द्वंद्व देखा गया। कंपनी ने अपने भारतीय समकक्षों के मुकाबले जवाबदेही के बिना अधिकार का इस्तेमाल किया, जिन पर जिम्मेदारी का भार था लेकिन उनके पास अनुरूप अधिकार का अभाव था।
इस द्वंद्व का परिणाम यह हुआ:
- कंपनी के कर्मियों में व्यापक भ्रष्टाचार।
- अत्यधिक राजस्व वसूली और किसानों की अधीनता।
- कंपनी की वित्तीय दिवालियापन, उसके कर्मियों की समृद्धि के विपरीत थी।
- ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया: इस क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था के जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने कानूनी ढांचे के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से कंपनी को विनियमित करने का विकल्प चुना।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किये गये अधिनियम
1773 का विनियमन अधिनियम:
- कंपनी की क्षेत्रीय हिस्सेदारी संरक्षित: इस कानून ने कंपनी को कंपनी के संचालन और कार्यक्षमता की निगरानी के उद्देश्य से भारत में अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बनाए रखने की मंजूरी दी।
- भारतीय मामलों की देखरेख: इस डिक्री के माध्यम से, ब्रिटिश कैबिनेट को पहली बार भारतीय मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया।
- मुख्य कार्यकारी का परिचय: इसने बंगाल के राज्यपाल के पद को “बंगाल के गवर्नर-जनरल” में बदल दिया।
- बंगाल में शासन का क्रियान्वयन गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा किया जाना था।
- वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर-जनरल की प्रारंभिक भूमिका निभाई।
- इसके बाद बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन काम करने लगे।
- सर्वोच्च न्यायालय की संस्था: अपीलीय न्यायक्षेत्रों के साथ बंगाल (कलकत्ता) में एक सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय स्थापित किया जाना था, जहाँ सभी विषय निवारण की मांग कर सकते थे।
- इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
- 1781 में, अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे गवर्नर-जनरल, काउंसिल और सरकार के कर्मियों को अधिकार क्षेत्र से छूट मिल गई यदि उनके कार्य उनके कर्तव्यों के दायरे में थे।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784:
- दोहरी निगरानी रूपरेखा: इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निगरानी की दोहरी प्रणाली स्थापित की।
- कंपनी ने राज्य के एक अधीनस्थ विभाग का दर्जा ग्रहण किया, और भारत में इसके क्षेत्रों को ‘ब्रिटिश संपत्ति’ का नाम दिया गया।
- फिर भी, इसने वाणिज्य और दैनिक प्रशासन पर नियंत्रण बरकरार रखा।
शासन प्राधिकरणों का गठन:
कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए एक नियामक संस्था की स्थापना की गई, जिसे नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल है:
- राजकोष के चांसलर
- राज्य के एक सचिव
- प्रिवी काउंसिल के चार सदस्य (क्राउन द्वारा नियुक्त)
महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों को ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा संचार बनाए रखने के लिए तीन निदेशकों की एक गोपनीय समिति को सौंप दिया गया था, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता था।
1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों के अधिकार प्रदान किये गये। यदि वह विकल्पों की जिम्मेदारी लेता है तो वह परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है।
चार्टर अधिनियम, 1793:
- गवर्नर-जनरल के लिए प्राधिकरण का विस्तार: इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दिए गए अधिभावी अधिकार को विस्तृत कर दिया, और इसे भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलों और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया।
- वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति: गवर्नर-जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य हो गया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया; ऐसी कार्रवाई को इस्तीफा माना गया।
- अधिकारियों के लिए मुआवज़ा: इसमें यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से पारिश्रमिक दिया जाएगा (यह 1919 तक जारी रहा)। इसके अतिरिक्त, कंपनी आवश्यक खर्चों को कवर करने के बाद ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का योगदान देने के लिए बाध्य थी।
चार्टर अधिनियम, 1813:
- अंग्रेजी व्यापारियों की अपील : अंग्रेजी व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी के लिए आग्रह किया, जो मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली से होने वाले व्यापार घाटे से प्रेरित था, जो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए बनाई गई थी।
- कंपनी के विशिष्ट अधिकारों का अंत: इस अधिनियम ने कंपनी से उसके विशेष वाणिज्यिक विशेषाधिकार छीन लिए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति पर ‘क्राउन की निर्विवाद संप्रभुता’ स्थापित हो गई। हालाँकि, कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा।
- जानकार स्थानीय लोगों के लिए सहायता: साहित्य के पुनरोद्धार, शिक्षित भारतीय व्यक्तियों के प्रोत्साहन और भारतीयों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति के लिए 1,00,000 रुपये का वार्षिक आवंटन निर्धारित किया गया था। इसने शिक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने की दिशा में प्रारंभिक प्रगति को चिह्नित किया।
चार्टर अधिनियम, 1833:
- कंपनी की व्यापार व्यवस्थाएँ: क्षेत्रीय नियंत्रण और राजस्व संग्रह के लिए कंपनी को दी गई 20 साल की लीज (चार्टर अधिनियम, 1813 के अनुसार) का विस्तार बढ़ा दिया गया था।
- फिर भी, चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी के विशेष अधिकार समाप्त कर दिये गये।
- यूरोपीय प्रवासन: भारत में यूरोपीय आप्रवासन और संपत्ति अधिग्रहण पर सभी सीमाएं हटा दी गईं, जिससे भारत में व्यापक यूरोपीय उपनिवेशीकरण की सुविधा मिल गई।
- भारत के गवर्नर-जनरल का परिचय: बंगाल के गवर्नर-जनरल की उपाधि को “भारत के गवर्नर-जनरल” में बदल दिया गया। प्राधिकार से संपन्न, गवर्नर-जनरल कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख, नियंत्रण और निर्देशन करता था। सभी राजस्व उसके दायरे में उत्पन्न होते थे, और वह व्यय पर पूरी निगरानी रखता था। विलियम बेंटिक ने भारत के गवर्नर-जनरल की प्रारंभिक भूमिका निभाई।
- विधि आयोग की स्थापना: भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए इस अधिनियम के तहत स्थापित, इसने भारत के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी मामलों में विशेषज्ञता वाला एक चौथा सामान्य सदस्य पेश किया। लॉर्ड मैकाले इस भूमिका के लिए पहले नियुक्त व्यक्ति थे।
चार्टर अधिनियम, 1853:
- कंपनी का व्यापार परिदृश्य : जब तक संसद द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, कंपनी ने क्षेत्रों पर कब्ज़ा बरकरार रखा। सेवाओं पर कंपनी का प्रभाव खत्म कर दिया गया और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल दिया गया।
- चौथे साधारण सदस्य का समावेश: कानून सदस्य ने गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की।
- भारतीय विधान परिषद: भारतीय विधानमंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। हालाँकि, गवर्नर-जनरल के पास विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने की शक्ति थी, जिससे कानूनों के अधिनियमन के लिए उनकी सहमति आवश्यक हो जाती थी।
भारत सरकार अधिनियम, 1858:
- 1857 के विद्रोह के बाद: 1857 के विद्रोह से जटिल परिस्थितियों से निपटने में कंपनी की सीमाएँ उजागर हो गईं। इस उथल-पुथल ने भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार छीनने का अवसर पैदा कर दिया।
- कंपनी प्रशासन का अंत: पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित दोहरी प्रणाली समाप्त हो गई, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां भारत को एक राज्य सचिव और 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाएगा। एक सलाहकार भूमिका.
- वायसराय का परिचय: भारत के गवर्नर-जनरल की उपाधि को वायसराय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे उपाधि धारक की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, हालांकि जरूरी नहीं कि उनका अधिकार हो। वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय के रूप में कार्यरत थे।
कंपनी शासन के दौरान गवर्नर-जनरल के अधीन सुधार :
लॉर्ड कार्नवालिस (गवर्नर-जनरल, 1786-93)
उन्होंने सिविल सेवाओं की स्थापना और संगठन की शुरुआत की। फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट अदालतें स्थापित की गईं।
कॉर्नवालिस कोड: इस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग करने की शुरुआत की, जिससे यूरोपीय विषयों को अधिकार क्षेत्र में लाया गया। सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्यों के लिए नागरिक अदालतों के प्रति जवाबदेह बन गए, जिससे कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित हुआ।
विलियम बेंटिक (गवर्नर-जनरल, 1828-1833)
उन्होंने चार सर्किट कोर्टों को नष्ट कर दिया और उनके कार्यों को कलेक्टरों को सौंप दिया। ऊपरी प्रांतों में लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत की स्थापना की गई।
अदालतों की आधिकारिक भाषा के रूप में फ़ारसी की जगह अंग्रेजी ने ले ली, और दावेदारों को फ़ारसी या स्थानीय भाषा का उपयोग करने का विकल्प दिया गया। कानूनों के संहिताकरण के परिणामस्वरूप एक सिविल प्रक्रिया संहिता (1859), एक भारतीय दंड संहिता (1860), और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861) तैयार की गई।
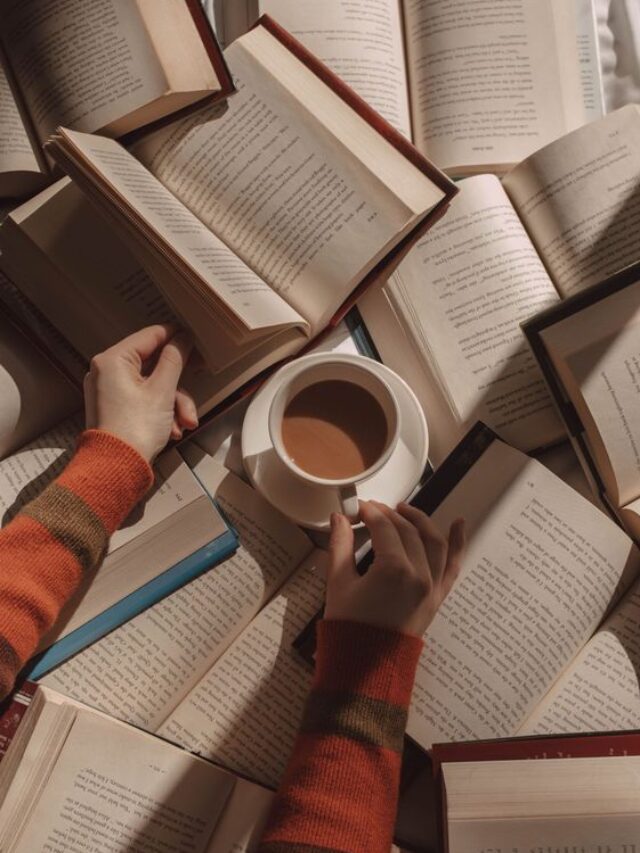


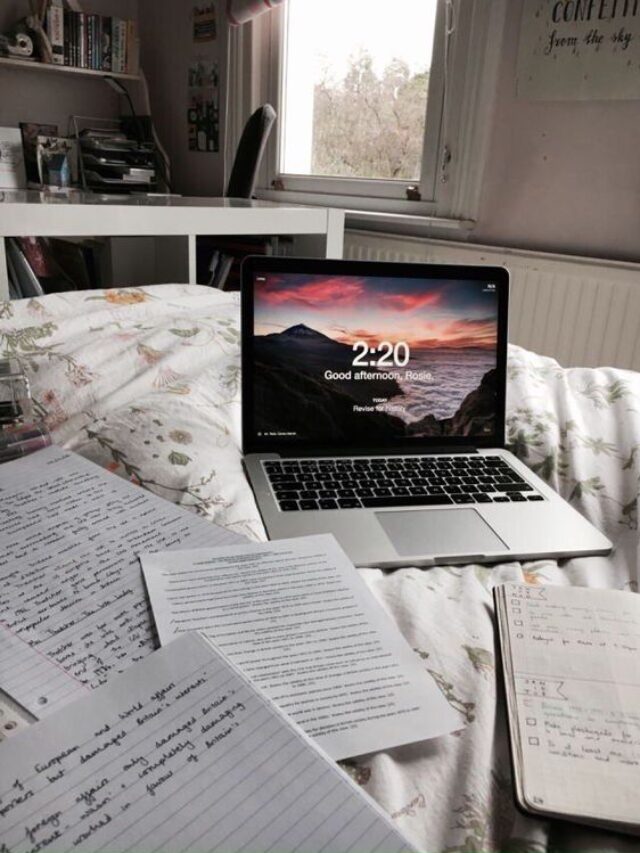

Leave a Reply