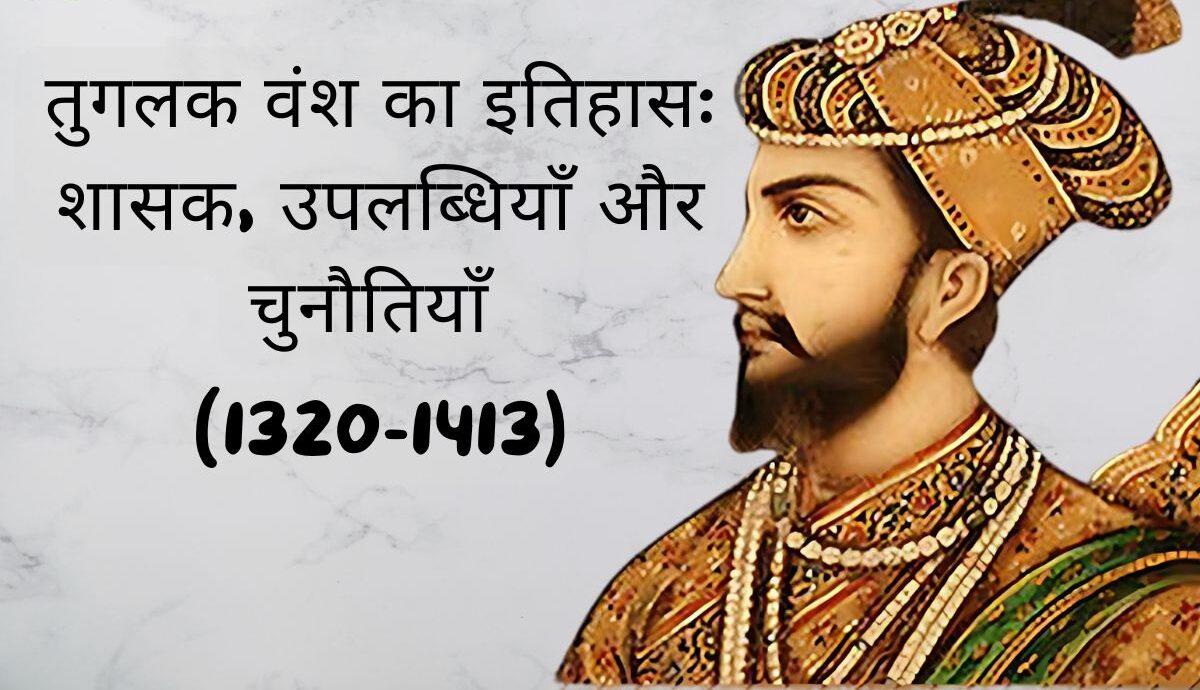
तुगलक वंश मध्ययुगीन भारत में उभरा और तुर्क या तुर्क-मंगोल मूल का था। 1320 से 1413 तक, राजवंश ने विभिन्न शासकों को देखा, जिनमें मुहम्मद बिन तुगलक और गाजी मलिक शामिल थे। तुगलक वंश के आक्रमण ने भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यह लेख तुगलक वंश और उसके शासकों से संबंधित भारतीय मध्ययुगीन इतिहास पर नोट्स का संदर्भ प्रदान करता है।
इतिहास
खिलजी वंश के बाद, तुगलक वंश ने 1320 से 1413 तक दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। इस अवधि ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण युग को चिह्नित किया।
कारखानों की स्थापना से आर्थिक गतिविधियाँ फली-फूलीं और सिंचित नहरों की शुरूआत से कृषि को बढ़ावा मिला। अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार दोनों फले-फूले, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो गई। शहरी केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
तुगलक वंश के प्रमुख शासक
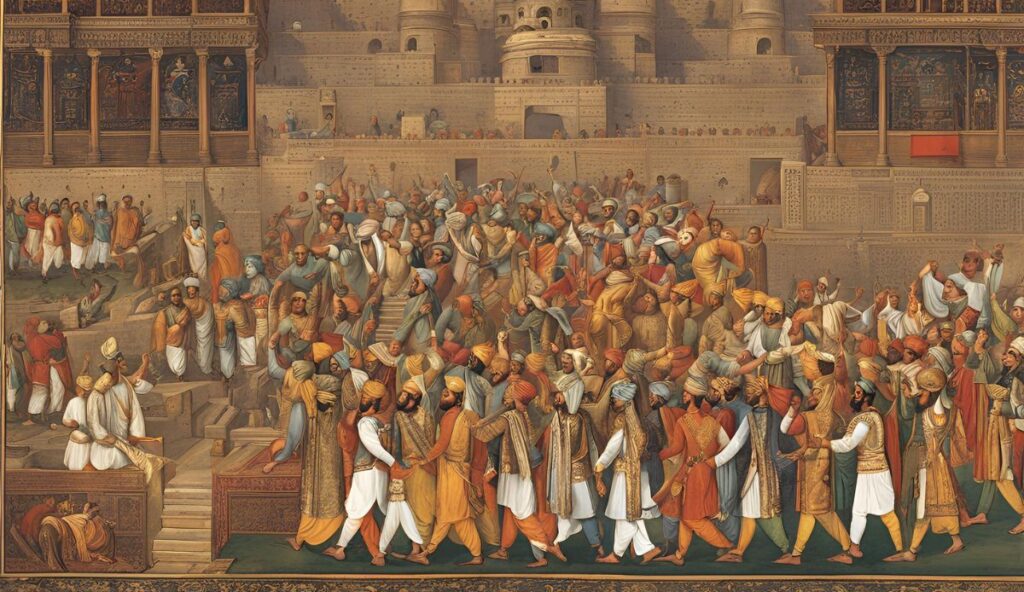
गयासुद्दीन तुगलक (गाजी मलिक)
- तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी, जो 1320 ई. में गयासुद्दीन तुगलक बन गया।
- थोड़े शासनकाल के बाद 1325 ई. में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र मुहम्मद तुगलक ने सत्ता संभाली।
- तुगलक शासन के दौरान, दिल्ली सल्तनत अधिक मजबूत हो गई, कई बाहरी क्षेत्र सीधे उसके नियंत्रण में आ गए।
- गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद के किलेदार शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसे राजधानी और रक्षा के लिए एक मजबूत किले दोनों के रूप में डिजाइन किया गया था।
मुहम्मद बिन तुगलक
- अपने पिता की मृत्यु के बाद, मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, हालाँकि कुछ इतिहासकारों ने उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया।
- राजत्व के दैवीय अधिकार सिद्धांत को अपनाते हुए, उन्होंने जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना अधिकारियों की नियुक्ति में उदार दृष्टिकोण अपनाया।
- उनके शासन ने अपनी हिंदू प्रजा के प्रति कोई पक्षपात नहीं दिखाया।
- विजय की नीति को लागू करते हुए, उन्होंने खुरासान, नगरकोट, करजाल, मेवाड़, तेलंगाना और मालाबार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभियान भेजे।
- कई एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद, उनका साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे व्यापक हो गया।
- उनके शासनकाल के दौरान उल्लेखनीय निर्माणों में जहांपनाह का शाही निवास और बेगमपुरी मस्जिद शामिल हैं।
फ़िरोज़ शाह तुगलक
- मुहम्मद तुगलक के चचेरे भाई, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1351 में सिंहासन ग्रहण किया और 1388 तक शासन किया।
- अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक दुर्जेय सैन्य नेता न होते हुए भी, सुल्तान ने खुद को शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक संरचनाओं के एक विपुल निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित किया।
- उन्होंने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत चार करों को लागू किया, जिसमें गैर-मुसलमानों पर कर भी शामिल था।
- 1361 में जाजनगर (ओडिशा) में उनके अभियान के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर का विनाश हुआ।
फ़िरोज़ शाह तुगलक की उपलब्धियाँ
फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और विभिन्न उपलब्धियां हासिल कीं:
- दीवान-ए-खैरात : दान के लिए एक कार्यालय की स्थापना की।
- दीवान-ए-बुंदगान: दासों के लिए एक विभाग बनाया गया।
- सराय (विश्राम गृह): व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए विश्राम स्थलों का निर्माण किया गया।
- चार नए शहर: फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना की।
नहर निर्माण:
- यमुना से लेकर हिसार शहर तक।
- सतलुज से घग्गर तक।
- घग्गर से फिरोजाबाद.
- हरियाणा में मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियां से हांसी तक।
लगाए गए कर:
- खराज : भूमि की उपज के दसवें हिस्से के बराबर भूमि कर।
- ज़कात: मुसलमानों से संपत्ति पर वसूला जाने वाला ढाई प्रतिशत कर।
- खम: पकड़ी गई लूट का पांचवां हिस्सा (सैनिकों के लिए आवंटित चार-पांचवां हिस्सा)।
- अन्य कर: इसमें सिंचाई कर, उद्यान कर, चुंगी कर और बिक्री कर शामिल हैं।
मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग
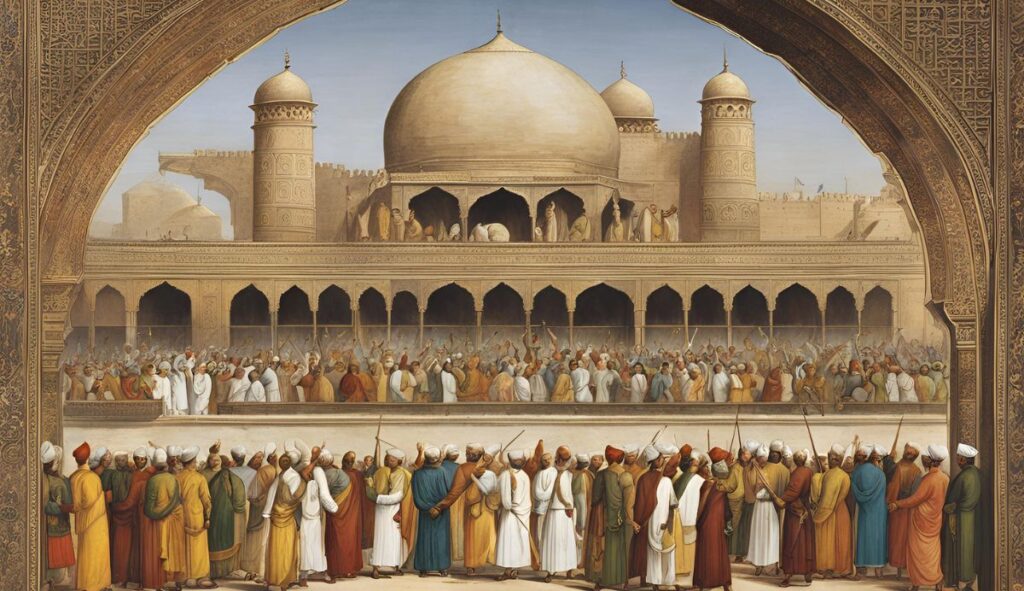
पूंजी का स्थानांतरण
- मुहम्मद बिन तुगलक (1324 – 1351) अपने साहसिक प्रयोगों के लिए उल्लेखनीय हैं, जिनमें से एक सबसे विवादास्पद है राजधानी को दिल्ली से देवगीर (बाद में इसका नाम दौलताबाद) में स्थानांतरित करना।
- इस कदम में केवल उच्च वर्ग शामिल थे, जिनमें शेख, रईस और उलेमा शामिल थे, जबकि सामान्य आबादी दिल्ली में ही रही।
- अंततः, दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का एहसास करते हुए, सुल्तान ने दौलताबाद को छोड़ दिया, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा मिला।
सांकेतिक मुद्रा
- सुल्तान की विजय योजनाओं से खाली खजाने के कारण एक और साहसी परियोजना “सांकेतिक मुद्रा” की शुरूआत थी।
- वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी के कारण, चांदी के टंका के स्थान पर तांबे के सिक्के (जित्तल) जारी किए गए, जिन्हें समकक्ष घोषित किया गया।
- हालाँकि, यह अवधारणा व्यापारियों और जनता के लिए नई और चुनौतीपूर्ण थी।
- जालसाजी बड़े पैमाने पर हो गई, और शाही सिक्कों को नकली सिक्कों से अलग करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा।
सैन्य अभियान
- 14वीं शताब्दी की शुरुआत में, मुहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए सैन्य उपक्रमों में लगी हुई थी।
- खुरासान अभियान का लक्ष्य अधिक सुरक्षित पश्चिमी सीमाएँ स्थापित करना था लेकिन यह सफल नहीं हुआ।
- कराचिल अभियान ने चीन से प्रभावित पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की।
- दुर्भाग्य से, यह अभियान असफल रूप से समाप्त हो गया। इस झटके के बावजूद चीन और दिल्ली के बीच राजनयिक चैनल खुल गए।
कृषि सुधार
- मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान, विभिन्न कृषि सुधार लागू किए गए, जो मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र पर केंद्रित थे।
- अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण के विपरीत, मुहम्मद तुगलक का लक्ष्य राज्य के लिए भूमि राजस्व का पर्याप्त हिस्सा सुनिश्चित करते हुए खुत और मुकद्दम (ग्राम प्रधान) की भूमिका को बनाए रखना था।
- दुर्भाग्य से, उनके शासन के दौरान इन उपायों के गंभीर परिणाम हुए।
- अति-मूल्यांकन के कारण गंगा के दोआब में एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह भड़क उठा, जिसके कारण किसानों को अपने गाँवों से भागना पड़ा।
- मुहम्मद तुगलक ने विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का प्रयास करते हुए कठोर प्रतिक्रिया दी। क्षेत्र में लंबे समय तक अकाल रहने से स्थिति और खराब हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर पीड़ा और मौतें हुईं।
- खेती में सुधार के प्रयास में, मुहम्मद तुगलक ने दोआब में कृषि को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की।
- उन्होंने इस उद्देश्य के लिए दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक एक समर्पित विभाग की स्थापना की। इस योजना में क्षेत्र को विकास खंडों में विभाजित करना शामिल था, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधिकारी द्वारा किया जाता था जिसे ऋण और प्रोत्साहन के माध्यम से बेहतर फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया था।
हालाँकि, इसे लागू करने के लिए नियुक्त लोगों की अनुभवहीनता और बेईमानी के कारण यह योजना विफल हो गई। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी फिरोज ने ऋण माफ कर दिया। फिर भी, मुहम्मद तुगलक द्वारा प्रस्तावित खेती नीति को फ़िरोज़ के तहत और भी महत्वपूर्ण रूप से, बाद में अकबर के शासनकाल के दौरान नवीनीकृत शक्ति मिली।
चुनौतियां
- मुहम्मद तुगलक को अपने कुलीन वर्ग के भीतर विविधता के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। चहलगानी तुर्कों के पतन और खलजियों के प्रभुत्व के बाद, कुलीन वर्ग में विभिन्न पृष्ठभूमियों के मुसलमान शामिल थे, जिनमें धर्मांतरित भारतीय भी शामिल थे।
- दिलचस्प बात यह है कि मुहम्मद तुगलक ने नाई, रसोइया, बुनकर और शराब बनाने वालों जैसे गैर-कुलीन पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कार्यालयों में नियुक्त किया। उनके कुलीन वर्ग में धर्मांतरित मुस्लिमों के वंशज, कुछ हिंदू और विदेशी नियुक्त लोग शामिल थे। इस विविध रचना के परिणामस्वरूप कुलीनों में एकता और निष्ठा की कमी हो गई।
- व्यापक साम्राज्य ने विद्रोह और अधिकार के स्वतंत्र क्षेत्रों की स्थापना के अवसर प्रदान किए, जो मुहम्मद तुगलक की कठोर सज़ाओं से और भी बदतर हो गए। नतीजतन, उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का शिखर और उसके विघटन की शुरुआत दोनों हुई।
- मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान उथल-पुथल भरे दौर के बाद फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया। पूरे साम्राज्य में विद्रोह भड़क उठे, विशेषकर दक्षिण भारत में, स्थानीय गवर्नरों द्वारा संगठित होकर शाही सेनाओं पर दबाव डाला गया।
- विनाशकारी प्लेग के कारण मुहम्मद तुगलक की सेना और कमजोर हो गई, जिससे दो-तिहाई सेना की मृत्यु हो गई। समवर्ती रूप से, दक्षिण में विद्रोहों के परिणामस्वरूप विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों की स्थापना हुई, साथ ही बंगाल को स्वतंत्रता मिली। अवध, गुजरात और सिंध में विद्रोह को दबाने के बावजूद, मुहम्मद तुगलक की सिंध में मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई फ़िरोज़ तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना।
- मुहम्मद तुगलक की विभाजनकारी नीतियों के बाद फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सत्ता संभालने के बाद, फ़िरोज़ ने अधिक प्रबंधनीय क्षेत्रों पर अधिकार जताते हुए रईसों, सेना और धार्मिक हस्तियों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। विशेष रूप से, उन्होंने दक्षिण भारत और दक्कन पर पुनः नियंत्रण न करने का विकल्प चुना।
- फ़िरोज़ तुगलक, हालांकि एक प्रसिद्ध सैन्य नेता नहीं था, अपने शासनकाल के दौरान शांति और क्रमिक विकास का दौर लाया। उन्होंने स्थिरता को बढ़ावा देते हुए मृत कुलीनों के बेटों, दामादों और दासों को पदों के उत्तराधिकार और भूमि अनुदान की अनुमति देने वाला एक डिक्री पेश किया।
- रईसों का पक्ष पाने के लिए, उन्होंने विद्रोह को कम करते हुए, खाता लेखा परीक्षा के दौरान उन्हें यातना देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। हालाँकि, वंशानुगत कार्यालयों और भूमि अनुदान की नीति में कमियाँ थीं, एक छोटे दायरे के बाहर भर्ती को सीमित करना और एक संकीर्ण समूह पर निर्भरता पैदा करना।
- फ़िरोज़ ने सेना में आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया, बूढ़े सैनिकों के स्थान पर उनकी संतानों को नियुक्त किया। सैनिकों को नकद के बजाय भू-राजस्व का कार्यभार मिलता था, जिसके कारण दीर्घकालिक समस्याएं जैसे कि ढीला सैन्य प्रशासन और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई।
- धर्मशास्त्रियों को खुश करने के लिए, फ़िरोज़ ने खुद को एक सच्चा मुस्लिम राजा घोषित किया और अपने राज्य की इस्लामी प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने न्यायपालिका और शैक्षणिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखते हुए कुछ धर्मशास्त्रियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया।
- फ़िरोज़ ने विद्वानों द्वारा गैर-इस्लामी समझी जाने वाली प्रथाओं का बहिष्कार किया और जजिया लगाने की पहल की। उन्होंने हिंदू विचारों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धार्मिक कार्यों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संगीत, चिकित्सा और गणित पर पुस्तकों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद की सुविधा प्रदान की।
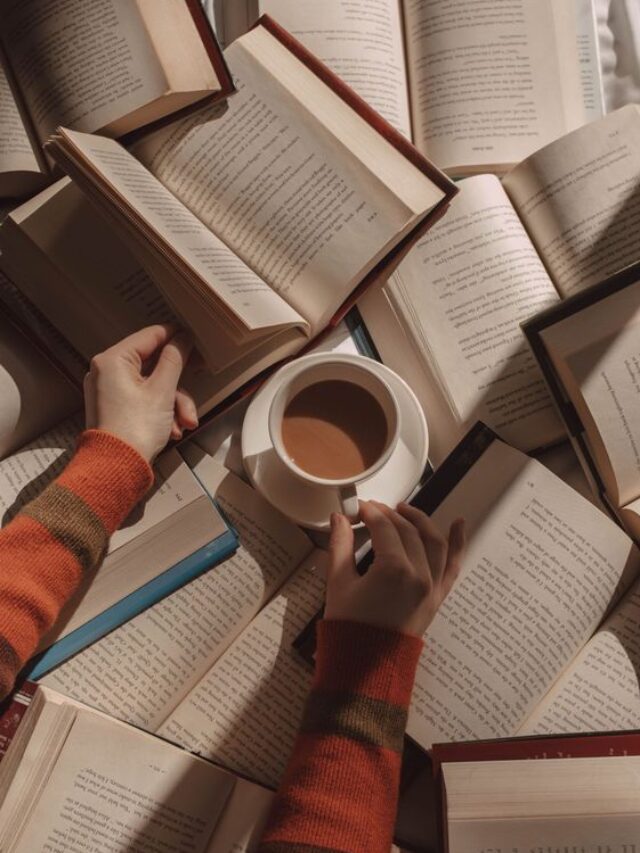


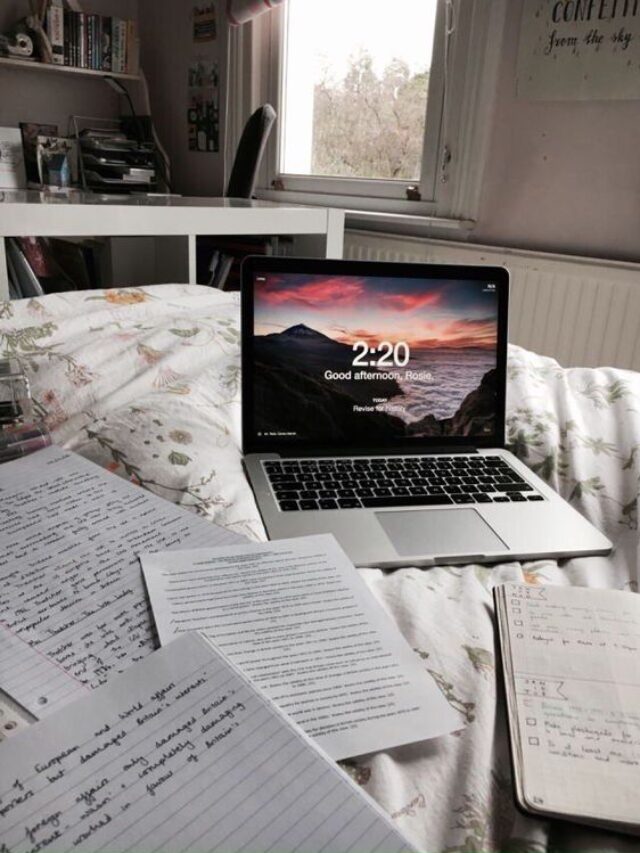
Leave a Reply