
ब्रिटिश भारत में न्यायिक ढांचे का उद्घाटन 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, जिसने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में दस्तावेजी अदालती उदाहरणों पर आधारित एक सामान्य कानून प्रणाली की स्थापना की थी। यह परिवर्तन तब हुआ जब कंपनी नए घटकों को पेश करते हुए एक वाणिज्यिक इकाई से एक शासक शक्ति के रूप में विकसित हुई। यह प्रवचन ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालता है और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालता है।
पृष्ठभूमि
पूर्व-औपनिवेशिक भारत में, मुगल काल और प्राचीन काल दोनों के दौरान, न्यायिक प्रणाली में उचित प्रक्रियाओं का अभाव था। कानून अदालतों में एक संरचित पदानुक्रम का अभाव था, और उनका वितरण उन क्षेत्रों के साथ संरेखित नहीं था जहां वे सेवा प्रदान करते थे। हिंदू कानूनी मामले आम तौर पर जमींदारों, स्थानीय पंचायतों या जाति के बुजुर्गों द्वारा हल किए जाते थे।
मुसलमानों के लिए, काजी, धार्मिक हस्तियों द्वारा धारण किया जाने वाला पद, न्यायिक प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था। ये कार्यालय प्रांतीय राजधानियों, कस्बों और बड़े गांवों (क़स्बा) में स्थित थे। राजाओं और बादशाहों द्वारा न्याय प्रदान करना मनमाना हो सकता है।
वॉरेन हेस्टिंग्स का युग
न्यायिक सुधारों के युग के दौरान, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के तहत:
जिला दीवानी अदालतें
- इनकी अध्यक्षता एक कलेक्टर द्वारा की जाती थी और मुस्लिम और हिंदू दोनों कानूनों द्वारा शासित नागरिक विवादों को संभाला जाता था। इन जिला-स्तरीय अदालतों से अपीलें सदर दीवानी अदालत को निर्देशित की गईं।
- समवर्ती रूप से, आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए काज़ियों और मुफ़्तियों की सहायता से एक भारतीय अधिकारी द्वारा प्रबंधित जिला फौजदारी अदालतें स्थापित की गईं।
- कलेक्टर ने इन अदालतों पर व्यापक नियंत्रण बनाए रखा, जो विशेष रूप से इस्लामी कानून को लागू करने के लिए नियोजित थे।
- मुर्शिदाबाद में सदर निज़ामत अदालत, एक उप निज़ाम की देखरेख और मुख्य क़ाज़ी और वरिष्ठ मुफ़्ती की सहायता से, मृत्युदंड और संपत्ति अधिग्रहण से निपटती थी।
- 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय दोनों ही ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों पर अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय के पास अपीलीय और मूल क्षेत्राधिकार दोनों थे।
लार्ड कार्नवालिस का काल
कॉर्नवालिस के तहत सुधार
- लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर-जनरल की भूमिका निभाई।
- 1787, 1790 और 1793 के वर्षों में, उन्होंने न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन लागू किया, जिसे सामूहिक रूप से 1787, 1790 और 1793 की न्यायिक योजना के रूप में जाना जाता है।
विलियम बेंटिक
विलियम बेंटिक के तहत सुधार
- गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक ने अपने प्रशासन के दौरान चार सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया।
- इन अदालतों के कर्तव्यों को कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया, जो राजस्व और सर्किट आयुक्त के मार्गदर्शन में उनकी देखरेख करते थे।
- इलाहाबाद में, ऊपरी प्रांतों के निवासियों की सुविधा के लिए विलियम बेंटिक द्वारा सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत की स्थापना की गई थी।
जबकि फ़ारसी अतीत में अदालतों की आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती थी, इन सुधारों के तहत, अदालती सत्र अब फ़ारसी या स्थानीय भाषा में आयोजित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अपनी सारी कार्यवाही अंग्रेजी में करता है।
ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास
1787 की न्यायिक योजना
- 1787 की न्यायिक योजना के तहत, कर और न्यायिक प्रणालियों को एकीकृत किया गया, जिससे कलेक्टर को दोनों पर नियंत्रण मिल गया।
- कलेक्टर, एक अंग्रेज अधिकारी, को कर लगाने और कर संबंधी मामलों को निपटाने का अधिकार था।
- कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जिलों की संख्या कम कर दी गई।
- लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरी तरह से आय के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्थानों पर माल अदालतें स्थापित कीं।
- राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख करने वाला कलेक्टर इन अदालतों की अध्यक्षता करता था।
- इन न्यायाधिकरणों की अपीलों पर पहले कलकत्ता में कर बोर्ड द्वारा और फिर काउंसिल में गवर्नर-जनरल द्वारा विचार किया गया।
- इसके अतिरिक्त, नागरिक विवादों को निपटाने वाली जिला दीवानी अदालतों का नेतृत्व कलेक्टर द्वारा किया जाता था। कलेक्टर के अधीनस्थ के रूप में छोटे नागरिक विवादों का प्रबंधन करने के लिए एक नया कार्यालय, रजिस्ट्रार कोर्ट बनाया गया था, जिसके लिए रजिस्ट्रार के आदेश को प्रभावी होने से पहले कलेक्टर की मंजूरी की आवश्यकता होती थी।
1790 की न्यायिक योजना
- 1790 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक न्याय को पुनर्गठित किया, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में समाप्त जिला फौजदारी अदालतों के स्थान पर सर्किट कोर्ट की स्थापना की।
- यूरोपीय न्यायाधीश इन अदालतों की अध्यक्षता करते थे, जो दीवानी और आपराधिक दोनों अपीलों को संभालते थे। सर्वोच्च आपराधिक अदालत, सदर निज़ामत अदालत को गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद की देखरेख में कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था।
1793 की न्यायिक योजना
- 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना जारी रखा।
- माल अदालतें, जहां कलेक्टर विशेष रूप से कर-संबंधित मामलों के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, का संचालन बंद हो गया।
- जिला दीवानी अदालतों ने इन राजस्व अदालतों से अधिकार और बकाया मामलों को ग्रहण किया।
- 1793 के कॉर्नवालिस कोड ने न्यायिक और राजस्व प्रबंधन को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। कलेक्टर अब न्यायिक अधिकार के बिना केवल कर संग्रहण का प्रबंधन करता था।
- जिला, शहर या जिला न्यायालय ने जिला दीवानी अदालत का स्थान ले लिया और इन अदालतों की देखरेख और मजिस्ट्रियल प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला न्यायाधीश का कार्यालय स्थापित किया गया।
- हिंदू और मुस्लिम कानून के लिए सिविल अदालतों का एक क्रम शुरू किया गया, जिसमें रजिस्ट्रार कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, चार सर्किट कोर्ट और कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत शामिल हैं।
- £5,000 या अधिक की अपील के लिए किंग-इन-काउंसिल से परामर्श की आवश्यकता होती है। कॉर्नवॉलिस कोड ने दिशानिर्देश निर्धारित किए, सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के लिए नागरिक अदालतों में जवाबदेह ठहराया, राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग किया और कानून की संप्रभुता स्थापित की।
ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली: 1833 का चार्टर अधिनियम
- 1833 के चार्टर अधिनियम ने लॉर्ड मैकाले की देखरेख में भारतीय कानून आयोग को जन्म दिया, जिसे भारतीय कानूनों को संकलित करने का काम सौंपा गया था। विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्य करते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता (1859), भारतीय दंड संहिता (1860), और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1862) तैयार की गई।
ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली: विकास
उच्च न्यायालयों की स्थापना
1834 और 1861 के बीच, भारत में अदालतों के दो अलग-अलग समूह थे – सदर अदालतें और सर्वोच्च न्यायालय – प्रत्येक का अपना क्षेत्राधिकार था। 1861 में, सिविल प्रक्रिया संहिता (1859), भारतीय दंड संहिता (1860), और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861) के पारित होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने न्याय प्रशासन में एकरूपता लाने की मांग की।
1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
- अगस्त 1861 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लागू किया, जिसमें बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में तीन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
- इस अधिनियम का उद्देश्य इन प्रेसीडेंसी में सदर अदालतों और सर्वोच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के साथ विलय करना था।
- बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के लिए चार्टर जून 1862 में जारी किए गए थे, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए चार्टर मई 1862 में जारी किए गए थे, जिससे यह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया।
- 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने क्राउन को ब्रिटिश भारत के भीतर अतिरिक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया।
- मार्च 1866 में, उत्तर-पश्चिमी प्रांत के लिए आगरा में सदर अदालत की जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो बाद में 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित हो गया, जो देश का पहला प्रांतीय उच्च न्यायालय बन गया।
- इसके बाद, अधिक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। फरवरी 1916 में, पटना उच्च न्यायालय बनाया गया था। 1919 में लाहौर में स्थापित पंजाब उच्च न्यायालय, आजादी के बाद शिमला और बाद में 1955 में चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया।
भारत का संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना की, जिसका कार्य प्रशासनों के बीच संघीय मुद्दों को हल करना था।
- 1937 में दिल्ली में गठित, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और छह से अधिक न्यायाधीश नहीं थे।
- अदालत ने मूल, अपीलीय और सलाहकार मामलों में क्षेत्राधिकार रखा, मुख्य रूप से प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच संघर्षों को हल किया, और उच्च न्यायालयों से सीमित अपीलों की सुनवाई की। इसने भारत के गवर्नर-जनरल को उसके अधिकार क्षेत्र के आधार पर सलाह दी।
- संघीय न्यायालय की अपीलों की सुनवाई लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा की जा सकती है।
- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, संघीय न्यायालय का नाम बदलकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार को समाप्त करने के लिए, संविधान सभा ने 1949 में प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम पारित किया।
- 28 जनवरी 1950 को स्थापित, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल और संघीय न्यायालय की न्यायिक समिति का स्थान ले लिया और भारतीय कानूनी प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय बन गया।
ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली: विकास
सकारात्मक पहलुओं
एक कानूनी प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें राजाओं के व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों को संहिताबद्ध कानूनों से बदल दिया गया। यहां तक कि यूरोपीय नागरिक भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। सरकारी कर्मचारी दीवानी अदालतों में उत्तरदायी हो गये।
नकारात्मक पहलु
कानूनी प्रणाली जटिल और महंगी हो गई, जिससे अमीरों को प्रभाव कायम करने की अनुमति मिल गई। चालाकी, धोखाधड़ी और धोखे के अवसर बढ़ गए। लंबी कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्याय में देरी हुई और अदालतें बढ़ती मुकदमेबाजी से बोझिल हो गईं। यूरोपीय न्यायाधीशों को अक्सर भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों से परिचित होने का अभाव था।
निष्कर्ष
भारतीय कानून का विकास रीति-रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों से सामान्य कानून और धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे में परिवर्तित हुआ। शासक वर्गों के प्रभाव ने भारतीय न्यायपालिका के विकास को आकार दिया, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की मध्यस्थता से लेकर अंग्रेजी (ब्रिटिश) की निरंकुश मध्यस्थता तक।
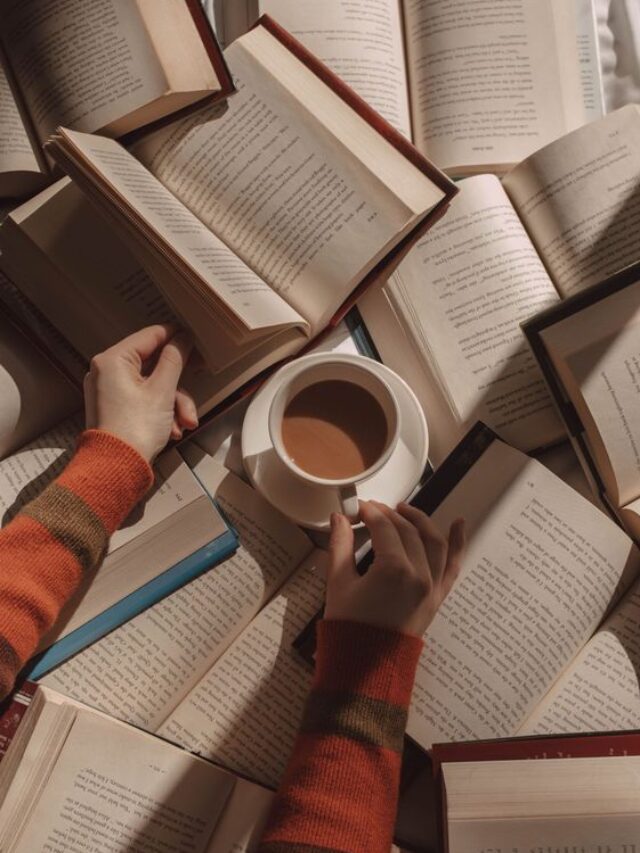


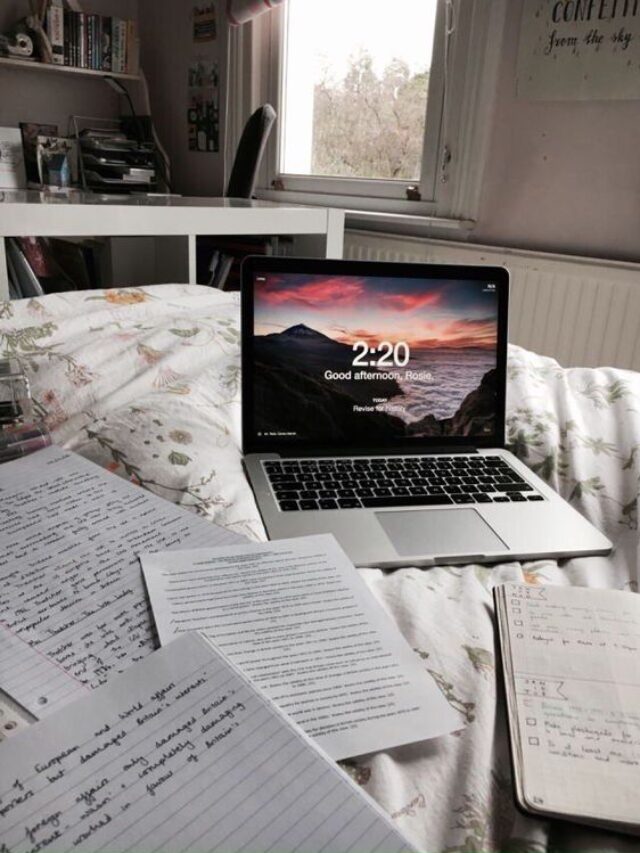

Leave a Reply